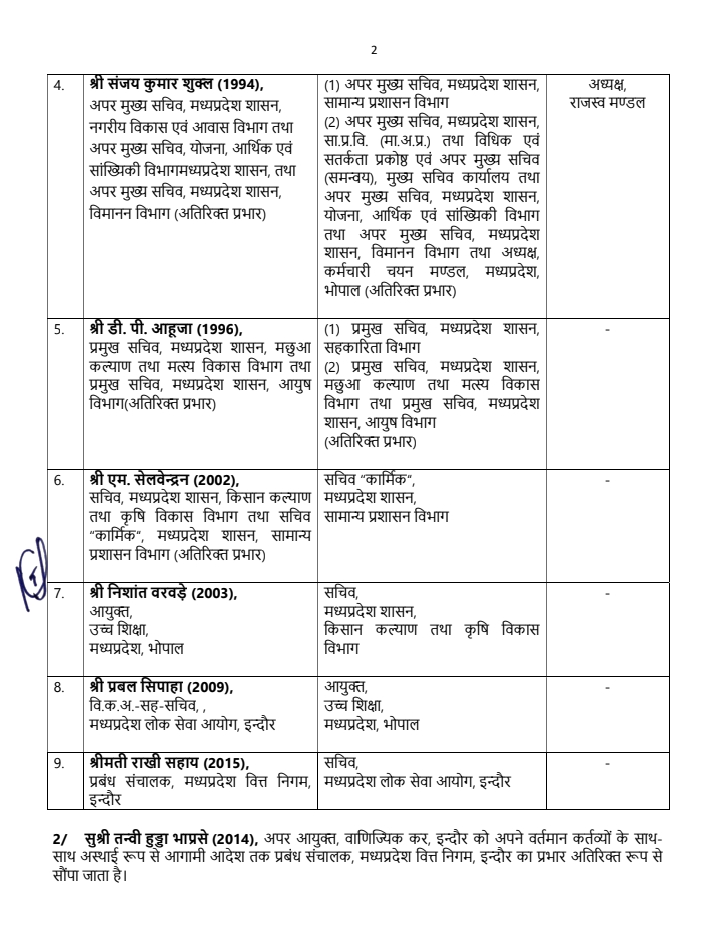ईरान संकट से उपजे बड़े सवाल

नया साल 2020 और नया दशक मध्य पूर्व में उभरते नए संकट के साथ शुरू हुआ है। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को दो जनवरी को बगदाद हवाई अड्डे के नजदीक अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला। इसके के बाद मध्य पूर्व में अशांति और तनाव बढ़ने लगा है। भारत के संदर्भ में बड़ा सवाल यह है कि इस हंगामे के आर्थिक और रणनीतिक सवाल क्या होंगे। कई सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 2012 में हुए हमलों में भी सुलेमानी का हाथ था।
दिल्ली में हमलों के दावे की हकीकत
ट्रंप ने हालांकि अपने बयान में भारत में सुलेमानी के हमले के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा नई दिल्ली में 13 फरवरी 2012 की उस वारदात की ओर था, जिसमें एक इजरायली राजनयिक की गाड़ी को उड़ा दिया गया था। इसमें उनकी पत्नी और ड्राइवर जख्मी हो गए थे। कार में चुंबक के सहारे बम फिट किया गया, जिसकी गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई और न ही भारत ने कभी उसके पीछे ईरान का हाथ बताया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि तेहरान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की हत्या के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने विस्फोट कराए। इस मामले में एक भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को पकड़ा गया, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी। जिन अन्य पांच के नाम सामने आए, वे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।
आर्थिक सुस्ती के बीच नई चुनौती
एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। इस बीच अमेरिका बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर उभरा है। भारत की तेल जरूरतों के करीब 10 फीसद की आपूर्ति अमेरिका से होती है जबकि ईरान से आपूर्ति लगभग शून्य तक पहुंच गया है। सुलेमानी की हत्या की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमत में चार फीसद का उछाल आ गया। सोने-चांदी की कीमत बढ़ गई। 2019 में कच्चा तेल लगभग 35 फीसद महंगा हो चुका है। भारत अपनी जरूरत का 83 फीसद तेल आयात करता है। जाहिर है, इन हालात में पहले से आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही सरकार का सिरदर्द बढ़ सकता है।
खाड़ी में रणनीतिक हित
अमेरिका, भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन ईरान के साथ इसका आर्थिक-सभ्यतागत संबंध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में ईरान और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिश की। भारत सरकार ने कहा, ‘जरूरी है कि हालात काबू से बाहर नहीं जाएं। भारत ने लगातार संयम बरतने को तवज्जो दिया है और आगे भी यही करेगा।’ दरअसल भारत को अब चाबहार में अपने हितों को लेकर अमेरिका को आश्वस्त करने के लिए मशक्कत करनी होगी। चाबहार पर भारत को छूट देने को लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि इससे भारत अफगानिस्तान में जरूरी सामानों को निर्यात करने में सक्षम होगा जो काबुल के भी हित में है। अगर खाड़ी में तनाव बढ़ता है तो चाबहार परियोजना पर ग्रहण लग सकता है। दूसरे, खाड़ी में भारत के करीब 80 लाख लोग काम करते हैं। ये भारत के लिए विदेशी पूंजी का एक बड़ा स्रोत भी हैं। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने पर इन लोगों के वहां फंसने की आशंका भी रहेगी।
ईरान के साथ रिश्तों की नाजुक डोर
अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते पहले ही नाजुक दौर में हैं। अमेरिका की ताजा कार्रवाई से महज दो हफ्ते पहले ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर तेहरान गए थे। इस दौरान दोनों ही देश चाबहार बंदरगाह परियोजना को तेजी देने पर सहमत हुए थे। ईरान के साथ संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका ने भारत को चाबहार को विकसित करने की इस शर्त पर ‘छूट’ दी है कि ईरानी सेना रिवोलूशनरी गार्ड्स इस परियोजना में शामिल न हो।
अमेरिका और ईरान का संतुलन
आज ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं लेकिन एक वक्त में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में तल्खी आ गई। इसके बाद भारत को भी तेहरान के साथ अपने रिश्तों को लेकर संतुलन साधना पड़ा। तब से नई दिल्ली अमेरिका और इजरायल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को बरकरार रखते हुए तेहरान को भी साधे रखने की कोशिश करता है। ईरान के साथ भारत के रिश्तों की जटिलता सिर्फ अमेरिका और इजरायल की वजह से नहीं है। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी भी जगजाहिर है।